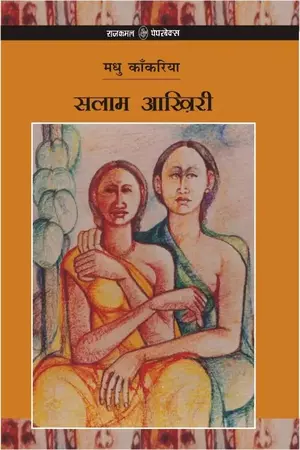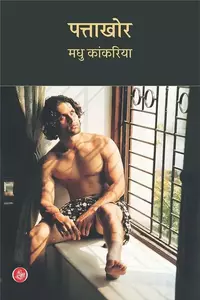|
उपन्यास >> सलाम आखिरी सलाम आखिरीमधु कांकरिया
|
177 पाठक हैं |
|||||||
समाज में वेश्या की मौजूदगी पर एक चिरन्तन सवाल...
Salam Aakhiri
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
समाज में वेश्या की मौजूदगी एक ऐसा चिरन्तन सवाल है जिससे हर समाज, हर युग में अपने-अपने ढंग से जूझता रहा है। वेश्या को कभी लोगों ने सभ्यता की जरूरत बताया, कभी कलंक बताया, कभी परिवार की किलेबंदी का बाई-प्रोडक्ट कहा और सभी सभ्य-सफेदपोश दुनिया का गटर जो ‘उनकी’ काम-कल्पनाओं और कुंठाओं के कीचड़ को दूर अँधेरे में ले जाकर डंप कर देता है। और, इधर वेश्याओं को एक सामान्य कर्मचारी का दर्जा दिलाए जाने की कवायद भी शुरू है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि समाज अपनी पूरी इच्छाशक्ति के साथ उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हो खड़ा हो जाए; तमाम तरह के उत्पीड़न-दमन और शोषण का शिकार वेश्याएँ उन्मूलन के नाम पर जरूर होती रही हैं।
यह उपन्यास वेश्याओं और वेश्यावृत्ति के पूरे परिदृश्य के देखते हुए हमारे भीतर उन असहाय स्त्रियों के प्रति करुणा का उद्रेक करने की कोशिश करता है, जो किसी भी कारण इस बदनाम और नरकीय व्यवसाय में आ फँसी हैं। कलकत्ता के सोनागाछी रेड लाइट एरिया की अँधेरी गलियों का सीधा साक्षात्कार कराते हुए लेखिका सभ्य समाज की संवेदनहीनता और कठोरता को भी साथ-साथ झिंझोड़ती चलती है; और यही चीज इस उपन्यास को सिर्फ एक कथा-पुस्तक की हद से निकालकर एक जरूरी किताब में बदल देती है।
यह उपन्यास वेश्याओं और वेश्यावृत्ति के पूरे परिदृश्य के देखते हुए हमारे भीतर उन असहाय स्त्रियों के प्रति करुणा का उद्रेक करने की कोशिश करता है, जो किसी भी कारण इस बदनाम और नरकीय व्यवसाय में आ फँसी हैं। कलकत्ता के सोनागाछी रेड लाइट एरिया की अँधेरी गलियों का सीधा साक्षात्कार कराते हुए लेखिका सभ्य समाज की संवेदनहीनता और कठोरता को भी साथ-साथ झिंझोड़ती चलती है; और यही चीज इस उपन्यास को सिर्फ एक कथा-पुस्तक की हद से निकालकर एक जरूरी किताब में बदल देती है।
आभार
संकल्प की निर्देशिका इन्द्राणी दी का, संलाप की सहायिका तप्ती ही का, मणिमाला राय, सम्पा दी और सभी स्टॉफ का।
कुसुम जैन, प्रमोद शाह, जय और द्वारिका जी का।
कुसुम जैन, प्रमोद शाह, जय और द्वारिका जी का।
आत्मकथ्य
इस विवेक-सम्पन्न समाज की निरन्तर बहती चेतना के प्रवाह में एक दीप की-सी आस्था के साथ प्रवाहित मेरा यह एक और उपन्यास-सलाम आख़िरी।
पिछले उपन्यास में मुझे आत्मकथ्य देने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वहा कोई द्वन्द्व न था, लेखिनी में कहीं कोई टकराव न था, कोई उलझन न थी, पर इस उपन्यास के दौरान लेखनी जैसे हाथों से छूट-छूट जाती थी। यहाँ पग-पग पर चुनौतियाँ थीं। प्रश्नों की नुकीली नोकें थीं। श्लीलता-अश्लीलता की चाबुकें थीं। संस्कार और संस्कृति के कठघरे थे। भाषा की अनावृत्ति का सवाल था। एक आत्मसंघर्ष। निरन्तर चलता रहा-क्या रहे लेखिका की लक्ष्मण रेखा ? वेश्याओं की जो दुनिया परत-दर-परत मेरी आँखों के समक्ष खुलती जा रही थी-उस दुनिया की कुरूपता, कुत्सा और भयानकता का चित्रण करने में लेखिका स्वयं को कितना डि-क्लास करे ?
उन्हीं दिनों या आत्मबोध हुआ कि क्यों कई विदेशी लेखकों तक ने इस विषय पर छद्म नाम से लिखा; पर इसके साथ ही एक वृहत्तर सत्य भी भीतर उतरता गया-‘जो बचेगा कैसे रचेगा’-(श्रीकांत वर्मा)। खैर....सभी किन्तु-परन्तु के उपरान्त इस दुनिया के सत्य हर छोर और सीमांतों को पकड़ने की कोशिश जारी रही।
उन्हीं दिनों किसी मित्र ने सुझाया कि मैं वेश्याओं के जीवन पर लिखी कुप्रिन की विश्वप्रसिद्ध कृति- ‘गाड़ीवालों का कटरा’ के हिन्दी अनुवाद की भूमिका अवश्य पढ़ लूँ। अनुवादक श्री चन्द्रभान जौहरी ने अपनी भूमिका में लिखा है कि भारत की स्थितियाँ भी उतनी ही भयावह और लगभग एक जैसी ही हैं जैसी कि कुप्रिन ने अपने उपन्यास में रूसी चकलाघरों की चित्रित की है। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहूँगी कि भारत में लालबत्ती इलाकों की स्थितियाँ कुप्रिन के चित्रण से न केवल भिन्न वरन् कहीं ज्यादा यांत्रिक, भयावह, कुत्सित एवं कुरूप हैं। बहुत संभव है कि श्री चन्द्रभान जौहरी पुरुष होने के कारण इस दुनिया की उन एकदम निचली तहों एवं बजबजाती हकीकतों तक नहीं पहुँच पाएँ हों, जहाँ स्त्री होने पर भी मुझे पहुँचने में जाने कितने शीर्षासन करने पड़े।
रूस में ही क्यों, भारत में भी उस समय जो वेश्या-जीवन था उसमें वेश्याएँ कम और ग्राहक ज्यादा हुआ करते थे, इस कारण वेश्याओं में फिर भी कुछ दम-खम बचा था, इसके अलावा वहां जीवन में देव-व्यापार के अलावा संगीत और नृत्य भी जुड़ा हुआ था। थोड़ा राग-रंग एवं हास-परिहास भी था। आज स्थिति विपरीत है। वेश्यावृत्ति एवं फ्लाईंग वेश्याएँ बढ़ रही हैं। आज वेश्याएँ बहुत ज्यादा हैं, ग्राहक कम हैं, इस कारण वेश्याएँ स्वयं को 20-20 रुपयों में मिनटों के हिसाब से नीलाम कर रही हैं। क्या कहा जाए इसे ? सभ्यता का अन्त या मनुष्यता का चरम पतन, कि आज देह की सजी दुकानों में देह एक डिपार्टमेंटल स्टोर बन गई है जहाँ नारी अपने अलग-अलग अंगों का घंटों और मिनटों के हिसाब से अलग-अलग सौदा कर रही है ! इस देह बाजार का इतना यंत्रीकरण हो चुका है कि सभी मानवीय अनुभूतियाँ और मर्यादाएँ स्वाहा हो चुकी हैं। मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम भेंट प्रेम वहाँ सामूहिक व्यभिचार में बदल चुका है। एक कमरे में तीन-तीन पुरुषों के साथ कोई एक भाड़े पर....बारी-बारी से। खुलेआम। इन्हीं लालबत्ती इलाकों में कहीं जगह की कमीं के चलते एक ही कमरे में कपड़ा टाँगकर.....।
कहीं पॉकेट में बीस का नोट लिए कोई स्कूली बालक इन बाजारों में। कहीं गाड़ी में बैठाकर कोई रईसजादा गाड़ी में ही..। इन सत्यों तक पहुँचने के लिए न सिर्फ परिक्रमाएँ लगानी पड़ीं, वरन् इनका विश्वास भी जीतना पड़ा जो कि कई बार बहुत ही जानलेवा साबित हुआ। वेश्याएँ अपने-अपने बारे में बताना नहीं चाहतीं, अपना सर्वस्व गँवाकर भी, अपनी इज्जत का ड़र अपने पेशे के खुलासा हो जाने का डर इनकी आत्मा से चिपका रहता है, विशेषकर जो आस-पास के गाँवों से आई हुई हैं, या जो पार्टटाइम या फ्लाईंग वेश्याएँ हैं।
दूसरी समस्या जो सामने आई वह थी इनकी भाषा को लेकर, कलकत्ता में प्राय: सभी वेश्याएँ, कुछेक नेपाली एवं आगरा वालियों को छोड़कर बंगालीभाषी हैं। अब इसे बंगला भाषा की समृद्धि कहा जाए, इस भूमि की तासीर कहा जाए या कि यहाँ के बंग साहित्य की अन्तर्शक्ति का कमाल कि अशिक्षित होते हुए भी यहाँ के सब्जीवाले, घरों में काम करनेवाली बाई, श्रमिक वगैरह भी आम हिन्दी भाषा से उच्च स्तर की भाषा बोलते हैं। वेश्याओं के लिए भी यही सत्य था। मुझे इनकी उच्च बंगाली को निम्न हिन्दी में रूपान्तरित करने की कवायद करनी पड़ी, पर अंतत: मुझसे यह कवायद सधी नहीं। इसी बिन्दु पर एक बार राजकमल प्रकाशन के संपादकीय विभाग ने भी ऐतराज जताया कि वेश्याएँ इतनी अच्छी भाषा कैसे बोल सकती हैं ? पांडुलिपि लौटा दी गई। खैर......
नारी का अर्थ यदि सृजन, प्रकृति और सम्पूर्णता है तो आज इस बाजार में तीनों नीलाम हो रहे हैं। और, यह नीलामी जीवन की नसतोड़ यंत्रणाओं और भुखमरी की कोख से उपजती है, जाने कैसे एक आम धारणा लोगों में है कि वेश्याएँ बहुत ठाट-बाट से रहने के लिए यह रास्ता अपनी इच्छा से पकड़ती हैं। यह सत्य उतना ही है जितना पहाड़ के सामने राई। 85 प्रतिशत वेश्यावृत्ति जीवन की चरम त्रासदी में भूख के मोर्चे के विरुद्ध अपनाई जाती है। 10 प्रतिशत वेश्यावृत्ति धोखाधड़ी से उपजती है, यह धोखाधड़ी प्रेम के झूठे वादे, नौकरी का प्रलोभन, शहरी चकाचौंध से लेकर एक उच्च और सम्मानित जीवन के सब्ज़बाग दिखाने तक होती है। असन्तुलित विकास, बेकारी, उजड़ते गाँव पारम्परिक शिल्प और घरेलू उद्योगों के विलुप्त हो जाने से शहरों की तरफ बढ़ता पलायन....आदि संभावनापूर्ण ‘इनपुट’ हैं इन लालबत्ती इलाकों के।
इन लालबत्ती इलाकों की संख्या खतरनाक गति से बढ़ रही है। पहले इने-गिने इलाके थे और वेश्याएँ भी शाम ढले निकलना शुरू होती थीं। आज इलाके बहुत बढ़ गए हैं, और सुबह से लेकर गहराती रात तक की गलियों के मुहाने पर ग्राहकों के इन्तजार में प्रतीक्षा करतीं और कमर दु:खाती जीवन से थकी-ऊबी, लिपी-पुती किशोरियाँ मिल जाएँगी। राष्ट्रीय महिला आयोग, 95-96 के अनुसार भारत के महानगरों में दस लाख से भी अधिक वेश्याएँ हैं पिछले साल से इसमें 20 प्रतिशत इजाफा हुआ है। इस समाचार पर गंभीर विचार करना तो दूर सम्भ्रान्त वर्ग यह मान बैठा है कि वेश्यावृत्ति बन्द नहीं हो सकती। एक बौद्धिक से पूछा गया, ‘क्या वेश्या उन्मूलन संभव है ? उसने जवाब दिया, ‘हाँ संभव है, पर वह उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार की ‘‘सोसाइटी विदाउट ए गटर।’’ इस भावशून्यता एवं भावनात्मक क्षरण के जवाब में यही कहा जा सकता है कि जनाब कभी यही तर्क दास प्रथा के लिए दिये जाते थे।
भगवान बचाए इस देश को, आज वेश्या-उन्मूलन, कम से कम सेकेंड़ जेनरेशन वेश्यावृत्ति, जीवन के दूसरे विकल्प, नयी शुरूआत की बातें तो दूर, कई नारी संगठन पुरजोर स्वरों में यह माँग उठा रहे हैं कि वेश्याओं को यौनकर्मी एवं श्रमिक का दर्जा दिया जाए और वेश्यावृत्ति को उद्योग का। कलकत्ते के साल्ट लेक स्टेडियम में फरवरी 2001 में वेश्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह देखकर मैं भौचक्क रह गई थी-इन संगठनों से मंत्र पाकर सभी वेश्याएँ अपने सीने पर ‘वी आर वर्कर्स’ का बैज लगाए स्वयं को गौरवान्वित कर रहीं थीं। यही मतिभ्रम स्वयं को ही उत्पाद बनाने की माँग, बाजार में ‘कॉमोडिटी’ बनने की आकांक्षा उन्हें किन अँधी सुरंगों में भटकाएगी ? इस पर गम्भीर विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार के संगठन नारी की अन्तर्निहित गरिमा एवं प्रेरणा के अन्त:स्रोत्रों को ही दाँव पर लगा रहे हैं !
पिछली सदी ने कई क्रान्तियाँ देखीं। आम आदमी को इँसान की गरिमा देने के लिए रूस, चीन, क्यूबा और वियतनाम में क्रान्तियाँ हुई, पर इन लालबत्ती इलाकों का अँधेरा घना ही होता जा रहा है क्योंकि इनमें आम आदमी समझा नहीं जाता है। महिला संगठन इन्हें उत्पाद बनाने पर तुले हैं। सरकारी खातों में ये भिखारियों के समक्ष हैं, इनकी आय पर कोई आयकर नहीं लगाया जाता क्योंकि यह अनैतिक ढंग से कमाया जाता है। वोट देने का अधिकार होने पर भी ये वोट नहीं दे पातीं क्योंकि सरकारी कर्मचारी इन गंदी एवं बदनाम गलियों में जाकर इनके नामों को सूची में डालने की जहमत नहीं उठाते और सबसे बढ़कर भद्र समाज इन्हें बुरी औरत एवं कुल्टा के रूप में देखता है। पर यह सोचने की बात है कि अधिकांश वेश्याएँ बारह-तेरह वर्ष की उम्र में ही इन गलियों में धकेल दी जाती हैं, कुछ यहीं आँख खोलती हैं। प्यार और संरक्षण से वंचित, अपने स्व और गहराइयों से दूर, ऐसी अर्द्धविकसित और अशिक्षित महिलाएँ, हर रात जिनकी देह का ही नहीं, आत्मा का भी चीरहरण होता हो, ऐसी महिलाएँ जीवन आस्था के आलोक-बिन्दु कहाँ से पाएँ जो स्त्री को स्त्री बनाते हैं ?
पिछले उपन्यास में मुझे आत्मकथ्य देने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वहा कोई द्वन्द्व न था, लेखिनी में कहीं कोई टकराव न था, कोई उलझन न थी, पर इस उपन्यास के दौरान लेखनी जैसे हाथों से छूट-छूट जाती थी। यहाँ पग-पग पर चुनौतियाँ थीं। प्रश्नों की नुकीली नोकें थीं। श्लीलता-अश्लीलता की चाबुकें थीं। संस्कार और संस्कृति के कठघरे थे। भाषा की अनावृत्ति का सवाल था। एक आत्मसंघर्ष। निरन्तर चलता रहा-क्या रहे लेखिका की लक्ष्मण रेखा ? वेश्याओं की जो दुनिया परत-दर-परत मेरी आँखों के समक्ष खुलती जा रही थी-उस दुनिया की कुरूपता, कुत्सा और भयानकता का चित्रण करने में लेखिका स्वयं को कितना डि-क्लास करे ?
उन्हीं दिनों या आत्मबोध हुआ कि क्यों कई विदेशी लेखकों तक ने इस विषय पर छद्म नाम से लिखा; पर इसके साथ ही एक वृहत्तर सत्य भी भीतर उतरता गया-‘जो बचेगा कैसे रचेगा’-(श्रीकांत वर्मा)। खैर....सभी किन्तु-परन्तु के उपरान्त इस दुनिया के सत्य हर छोर और सीमांतों को पकड़ने की कोशिश जारी रही।
उन्हीं दिनों किसी मित्र ने सुझाया कि मैं वेश्याओं के जीवन पर लिखी कुप्रिन की विश्वप्रसिद्ध कृति- ‘गाड़ीवालों का कटरा’ के हिन्दी अनुवाद की भूमिका अवश्य पढ़ लूँ। अनुवादक श्री चन्द्रभान जौहरी ने अपनी भूमिका में लिखा है कि भारत की स्थितियाँ भी उतनी ही भयावह और लगभग एक जैसी ही हैं जैसी कि कुप्रिन ने अपने उपन्यास में रूसी चकलाघरों की चित्रित की है। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहूँगी कि भारत में लालबत्ती इलाकों की स्थितियाँ कुप्रिन के चित्रण से न केवल भिन्न वरन् कहीं ज्यादा यांत्रिक, भयावह, कुत्सित एवं कुरूप हैं। बहुत संभव है कि श्री चन्द्रभान जौहरी पुरुष होने के कारण इस दुनिया की उन एकदम निचली तहों एवं बजबजाती हकीकतों तक नहीं पहुँच पाएँ हों, जहाँ स्त्री होने पर भी मुझे पहुँचने में जाने कितने शीर्षासन करने पड़े।
रूस में ही क्यों, भारत में भी उस समय जो वेश्या-जीवन था उसमें वेश्याएँ कम और ग्राहक ज्यादा हुआ करते थे, इस कारण वेश्याओं में फिर भी कुछ दम-खम बचा था, इसके अलावा वहां जीवन में देव-व्यापार के अलावा संगीत और नृत्य भी जुड़ा हुआ था। थोड़ा राग-रंग एवं हास-परिहास भी था। आज स्थिति विपरीत है। वेश्यावृत्ति एवं फ्लाईंग वेश्याएँ बढ़ रही हैं। आज वेश्याएँ बहुत ज्यादा हैं, ग्राहक कम हैं, इस कारण वेश्याएँ स्वयं को 20-20 रुपयों में मिनटों के हिसाब से नीलाम कर रही हैं। क्या कहा जाए इसे ? सभ्यता का अन्त या मनुष्यता का चरम पतन, कि आज देह की सजी दुकानों में देह एक डिपार्टमेंटल स्टोर बन गई है जहाँ नारी अपने अलग-अलग अंगों का घंटों और मिनटों के हिसाब से अलग-अलग सौदा कर रही है ! इस देह बाजार का इतना यंत्रीकरण हो चुका है कि सभी मानवीय अनुभूतियाँ और मर्यादाएँ स्वाहा हो चुकी हैं। मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम भेंट प्रेम वहाँ सामूहिक व्यभिचार में बदल चुका है। एक कमरे में तीन-तीन पुरुषों के साथ कोई एक भाड़े पर....बारी-बारी से। खुलेआम। इन्हीं लालबत्ती इलाकों में कहीं जगह की कमीं के चलते एक ही कमरे में कपड़ा टाँगकर.....।
कहीं पॉकेट में बीस का नोट लिए कोई स्कूली बालक इन बाजारों में। कहीं गाड़ी में बैठाकर कोई रईसजादा गाड़ी में ही..। इन सत्यों तक पहुँचने के लिए न सिर्फ परिक्रमाएँ लगानी पड़ीं, वरन् इनका विश्वास भी जीतना पड़ा जो कि कई बार बहुत ही जानलेवा साबित हुआ। वेश्याएँ अपने-अपने बारे में बताना नहीं चाहतीं, अपना सर्वस्व गँवाकर भी, अपनी इज्जत का ड़र अपने पेशे के खुलासा हो जाने का डर इनकी आत्मा से चिपका रहता है, विशेषकर जो आस-पास के गाँवों से आई हुई हैं, या जो पार्टटाइम या फ्लाईंग वेश्याएँ हैं।
दूसरी समस्या जो सामने आई वह थी इनकी भाषा को लेकर, कलकत्ता में प्राय: सभी वेश्याएँ, कुछेक नेपाली एवं आगरा वालियों को छोड़कर बंगालीभाषी हैं। अब इसे बंगला भाषा की समृद्धि कहा जाए, इस भूमि की तासीर कहा जाए या कि यहाँ के बंग साहित्य की अन्तर्शक्ति का कमाल कि अशिक्षित होते हुए भी यहाँ के सब्जीवाले, घरों में काम करनेवाली बाई, श्रमिक वगैरह भी आम हिन्दी भाषा से उच्च स्तर की भाषा बोलते हैं। वेश्याओं के लिए भी यही सत्य था। मुझे इनकी उच्च बंगाली को निम्न हिन्दी में रूपान्तरित करने की कवायद करनी पड़ी, पर अंतत: मुझसे यह कवायद सधी नहीं। इसी बिन्दु पर एक बार राजकमल प्रकाशन के संपादकीय विभाग ने भी ऐतराज जताया कि वेश्याएँ इतनी अच्छी भाषा कैसे बोल सकती हैं ? पांडुलिपि लौटा दी गई। खैर......
नारी का अर्थ यदि सृजन, प्रकृति और सम्पूर्णता है तो आज इस बाजार में तीनों नीलाम हो रहे हैं। और, यह नीलामी जीवन की नसतोड़ यंत्रणाओं और भुखमरी की कोख से उपजती है, जाने कैसे एक आम धारणा लोगों में है कि वेश्याएँ बहुत ठाट-बाट से रहने के लिए यह रास्ता अपनी इच्छा से पकड़ती हैं। यह सत्य उतना ही है जितना पहाड़ के सामने राई। 85 प्रतिशत वेश्यावृत्ति जीवन की चरम त्रासदी में भूख के मोर्चे के विरुद्ध अपनाई जाती है। 10 प्रतिशत वेश्यावृत्ति धोखाधड़ी से उपजती है, यह धोखाधड़ी प्रेम के झूठे वादे, नौकरी का प्रलोभन, शहरी चकाचौंध से लेकर एक उच्च और सम्मानित जीवन के सब्ज़बाग दिखाने तक होती है। असन्तुलित विकास, बेकारी, उजड़ते गाँव पारम्परिक शिल्प और घरेलू उद्योगों के विलुप्त हो जाने से शहरों की तरफ बढ़ता पलायन....आदि संभावनापूर्ण ‘इनपुट’ हैं इन लालबत्ती इलाकों के।
इन लालबत्ती इलाकों की संख्या खतरनाक गति से बढ़ रही है। पहले इने-गिने इलाके थे और वेश्याएँ भी शाम ढले निकलना शुरू होती थीं। आज इलाके बहुत बढ़ गए हैं, और सुबह से लेकर गहराती रात तक की गलियों के मुहाने पर ग्राहकों के इन्तजार में प्रतीक्षा करतीं और कमर दु:खाती जीवन से थकी-ऊबी, लिपी-पुती किशोरियाँ मिल जाएँगी। राष्ट्रीय महिला आयोग, 95-96 के अनुसार भारत के महानगरों में दस लाख से भी अधिक वेश्याएँ हैं पिछले साल से इसमें 20 प्रतिशत इजाफा हुआ है। इस समाचार पर गंभीर विचार करना तो दूर सम्भ्रान्त वर्ग यह मान बैठा है कि वेश्यावृत्ति बन्द नहीं हो सकती। एक बौद्धिक से पूछा गया, ‘क्या वेश्या उन्मूलन संभव है ? उसने जवाब दिया, ‘हाँ संभव है, पर वह उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार की ‘‘सोसाइटी विदाउट ए गटर।’’ इस भावशून्यता एवं भावनात्मक क्षरण के जवाब में यही कहा जा सकता है कि जनाब कभी यही तर्क दास प्रथा के लिए दिये जाते थे।
भगवान बचाए इस देश को, आज वेश्या-उन्मूलन, कम से कम सेकेंड़ जेनरेशन वेश्यावृत्ति, जीवन के दूसरे विकल्प, नयी शुरूआत की बातें तो दूर, कई नारी संगठन पुरजोर स्वरों में यह माँग उठा रहे हैं कि वेश्याओं को यौनकर्मी एवं श्रमिक का दर्जा दिया जाए और वेश्यावृत्ति को उद्योग का। कलकत्ते के साल्ट लेक स्टेडियम में फरवरी 2001 में वेश्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह देखकर मैं भौचक्क रह गई थी-इन संगठनों से मंत्र पाकर सभी वेश्याएँ अपने सीने पर ‘वी आर वर्कर्स’ का बैज लगाए स्वयं को गौरवान्वित कर रहीं थीं। यही मतिभ्रम स्वयं को ही उत्पाद बनाने की माँग, बाजार में ‘कॉमोडिटी’ बनने की आकांक्षा उन्हें किन अँधी सुरंगों में भटकाएगी ? इस पर गम्भीर विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार के संगठन नारी की अन्तर्निहित गरिमा एवं प्रेरणा के अन्त:स्रोत्रों को ही दाँव पर लगा रहे हैं !
पिछली सदी ने कई क्रान्तियाँ देखीं। आम आदमी को इँसान की गरिमा देने के लिए रूस, चीन, क्यूबा और वियतनाम में क्रान्तियाँ हुई, पर इन लालबत्ती इलाकों का अँधेरा घना ही होता जा रहा है क्योंकि इनमें आम आदमी समझा नहीं जाता है। महिला संगठन इन्हें उत्पाद बनाने पर तुले हैं। सरकारी खातों में ये भिखारियों के समक्ष हैं, इनकी आय पर कोई आयकर नहीं लगाया जाता क्योंकि यह अनैतिक ढंग से कमाया जाता है। वोट देने का अधिकार होने पर भी ये वोट नहीं दे पातीं क्योंकि सरकारी कर्मचारी इन गंदी एवं बदनाम गलियों में जाकर इनके नामों को सूची में डालने की जहमत नहीं उठाते और सबसे बढ़कर भद्र समाज इन्हें बुरी औरत एवं कुल्टा के रूप में देखता है। पर यह सोचने की बात है कि अधिकांश वेश्याएँ बारह-तेरह वर्ष की उम्र में ही इन गलियों में धकेल दी जाती हैं, कुछ यहीं आँख खोलती हैं। प्यार और संरक्षण से वंचित, अपने स्व और गहराइयों से दूर, ऐसी अर्द्धविकसित और अशिक्षित महिलाएँ, हर रात जिनकी देह का ही नहीं, आत्मा का भी चीरहरण होता हो, ऐसी महिलाएँ जीवन आस्था के आलोक-बिन्दु कहाँ से पाएँ जो स्त्री को स्त्री बनाते हैं ?
-मधु काँकरिया
परिक्रमाएँ- घूँघट के पट खोल
जिन दरवाजों से आज आपको लाया जा रहा है, ये वे दरवाजे हैं शहर के जो खुलते ही दुनिया में ले जाते हैं जिसके होने एवं जीवित रहने के विधान-वे नहीं हैं जो आप अपने घरों में देखते-सुनते हैं या अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं। सभ्यता के अनुशासन से परे, इस दुनिया के विधान दूसरे हैं, जीने की शर्तें अलग हैं। इंसान को छोटा करने वाले इन दरवाजों से गुजरते हुए आपके पिछले तमाम अनुभव इस परिदृश्य में आकर समाप्त हो जाते हैं, और यदि आप तनिक भी सोचने वाले जीव हुए और वक्त ने आपको पूरी तरह संवेदनाशून्य एवं आत्मविहीन नहीं बना डाला है तो केवल आप काल, समय और जिन्दगी पर अपनी राय बदलने को मजबूर होंगे वरन् आप भी वे नहीं रहेंगे जो इन दरवाजों में प्रवेश करने के पूर्व थे.....जिन्दगी के कई रंग जा चुके होंगे, बहुत कुछ बदल चुका होगा इस बीच।
यह वेश्याओं की एक रहस्यमय दुनिया है। शताब्दियों का बोझ ढोती हुई। देह के मन्दिरों और देह के पुजारियों की यह वह दुनिया है जो वितृष्णा में लिप्टी एक अजीब सा सम्मोहन जगाती है। यहाँ जिन्दगी का शोर-शराबा है, हर गली के हर कमरे का अलग-अलग इतिहास.....जहाँ हर रात देह की नहीं उघड़ती है वरन् आत्माओं का भी चीर-हरण होता रहता है।
यह दुनिया कलकत्ता महानगर के विभिन्न दरवाजों- सोनागाछी, बहु बाजार, कालीघाट, बैरकपुर, खिदिरपुर आदि में खुलती है। यहाँ जीवन के कुरुप से कुरुप एवं भयंकर से भयंकर नग्न रूप मिल जाएँगे क्योंकि यहाँ संस्कृति, मर्यादा एवं परम्पराओं का कोई डर नहीं है। बन्धन नहीं है। इस रूप के बाजार का रूप विहीन जीवन अपने चरम रूप में आपके समक्ष खुलते थान की तरह बेशर्मी से खुला हुआ है। इन सभी लालबत्ती इलाकों में सबसे प्राचीन, सबसे स्थगित, बदनाम, खासी आबादीवाला इतिहास और विरासत वाला इलाका है सोनगाछी।
तो सबसे पहले लीजिए एक जाम सोनागाछी के नाम !
कोई एक गुमसुम स्पन्दनहीन दोपहरी और ऐसे में सुरंग के समान लम्बी सँकरी और अँधेरी गली का मुहाना। और उस मुहाने पर खड़ी आठ-नौ ‘ऑन लाइन’ वेश्याएँ-‘बिकाऊ है’ की अदृश्य तख्ती लटकाए हुए।
अँधेरे और उम्मीद के सन्धिस्थल पर।
अपने स्वाभिमान के विरुद्ध।
अपने खिलाफ !
किसी दूसरी देह का इंतजार करती। उबकाईं और उदास।
लिपी-पुती देह। आँखों में भविष्यहीनता। चेहरे पर सस्ता और भड़कीला मेकअप। रँगे होंठ। सस्ती चमक के आभूषण। चटक और सस्ती किस्म की पोशांके। प्लास्टिक की चप्पलें। कहीं चमड़े़ की भी। प्रतीक्षा के लाखों कल्प। अठारह से लेकर चालीस-बयालीस की उम्र की लगभग सभी वारांगनाएँ। तरह-तरह की-बंगाली, नेपाली और आगरावाली।
एक नज़र में न हुस्न के जलवे। न अदाओं का जादू। न कला। न श्रृंगार। न साज, न आवाज।
सिर्फ देह, मादा देह !
ईश्वर की मानव को अमूल्य भेंट प्रेम और नारी सबसे मूल्यवान सम्पत्ति शील के खरीद-फरोख्त के ये रास्ते।
आसपास मँडराते कुछ लगुवे-भगुवे दलाल-चलता-फिरता ‘पूछताछ कार्यालय’ बने हुए।
‘‘सर, सर इधर चलिए....बस थोड़ा सा आगे, पटाखा माल है, जोरदार चीज। हाँ-हाँ सर, बस गारंटी ही समझिए......बस सर, एक बार देख लीजिए.....आप भी क्या याद रखेंगे !’’
शक्ल से बदतमीज दिखते हुए भी वह बड़े तमीज से पेश आ रहा था और एकाएक उसकी गोल-गोल गुलट्टी-सी लपलपाती आँखें धूप में चौंधियाते काँच-सी चमकने लगती हैं और दूसरे ही साँस से वह बोल पड़ता है।
आवाज का गियर बदला हुआ।
‘‘सर, सुनिए तो, अबकी-बहुत वैराइटी है। आगरावाली, नेपाली, बंगाली और सर....मोहम्डन भी है, खालिस मुसल्ली....कसम से सर, अरे झूठ क्यूँ बोलूँगा सर, और झूठ बोल भी दूँ तो भी क्या, सोलह साल की कुड़ी तो जवान होनी ही है....’’
‘‘क्या कहा.....? मोहम्डन भी है, तब तो हम जरूर जाएँगे....उसे पवित्र करने। यही तो जीत होगी हमारे ब्राह्मणत्व की।’’
और वे दोनों तेजी से उस अँधेरी सँकरी गली में घुस गए।
कुछ कदम और आगे ....
एक दूसरा दृश्य.....इसी से मिलता-जुलता।
यह वेश्याओं की एक रहस्यमय दुनिया है। शताब्दियों का बोझ ढोती हुई। देह के मन्दिरों और देह के पुजारियों की यह वह दुनिया है जो वितृष्णा में लिप्टी एक अजीब सा सम्मोहन जगाती है। यहाँ जिन्दगी का शोर-शराबा है, हर गली के हर कमरे का अलग-अलग इतिहास.....जहाँ हर रात देह की नहीं उघड़ती है वरन् आत्माओं का भी चीर-हरण होता रहता है।
यह दुनिया कलकत्ता महानगर के विभिन्न दरवाजों- सोनागाछी, बहु बाजार, कालीघाट, बैरकपुर, खिदिरपुर आदि में खुलती है। यहाँ जीवन के कुरुप से कुरुप एवं भयंकर से भयंकर नग्न रूप मिल जाएँगे क्योंकि यहाँ संस्कृति, मर्यादा एवं परम्पराओं का कोई डर नहीं है। बन्धन नहीं है। इस रूप के बाजार का रूप विहीन जीवन अपने चरम रूप में आपके समक्ष खुलते थान की तरह बेशर्मी से खुला हुआ है। इन सभी लालबत्ती इलाकों में सबसे प्राचीन, सबसे स्थगित, बदनाम, खासी आबादीवाला इतिहास और विरासत वाला इलाका है सोनगाछी।
तो सबसे पहले लीजिए एक जाम सोनागाछी के नाम !
कोई एक गुमसुम स्पन्दनहीन दोपहरी और ऐसे में सुरंग के समान लम्बी सँकरी और अँधेरी गली का मुहाना। और उस मुहाने पर खड़ी आठ-नौ ‘ऑन लाइन’ वेश्याएँ-‘बिकाऊ है’ की अदृश्य तख्ती लटकाए हुए।
अँधेरे और उम्मीद के सन्धिस्थल पर।
अपने स्वाभिमान के विरुद्ध।
अपने खिलाफ !
किसी दूसरी देह का इंतजार करती। उबकाईं और उदास।
लिपी-पुती देह। आँखों में भविष्यहीनता। चेहरे पर सस्ता और भड़कीला मेकअप। रँगे होंठ। सस्ती चमक के आभूषण। चटक और सस्ती किस्म की पोशांके। प्लास्टिक की चप्पलें। कहीं चमड़े़ की भी। प्रतीक्षा के लाखों कल्प। अठारह से लेकर चालीस-बयालीस की उम्र की लगभग सभी वारांगनाएँ। तरह-तरह की-बंगाली, नेपाली और आगरावाली।
एक नज़र में न हुस्न के जलवे। न अदाओं का जादू। न कला। न श्रृंगार। न साज, न आवाज।
सिर्फ देह, मादा देह !
ईश्वर की मानव को अमूल्य भेंट प्रेम और नारी सबसे मूल्यवान सम्पत्ति शील के खरीद-फरोख्त के ये रास्ते।
आसपास मँडराते कुछ लगुवे-भगुवे दलाल-चलता-फिरता ‘पूछताछ कार्यालय’ बने हुए।
‘‘सर, सर इधर चलिए....बस थोड़ा सा आगे, पटाखा माल है, जोरदार चीज। हाँ-हाँ सर, बस गारंटी ही समझिए......बस सर, एक बार देख लीजिए.....आप भी क्या याद रखेंगे !’’
शक्ल से बदतमीज दिखते हुए भी वह बड़े तमीज से पेश आ रहा था और एकाएक उसकी गोल-गोल गुलट्टी-सी लपलपाती आँखें धूप में चौंधियाते काँच-सी चमकने लगती हैं और दूसरे ही साँस से वह बोल पड़ता है।
आवाज का गियर बदला हुआ।
‘‘सर, सुनिए तो, अबकी-बहुत वैराइटी है। आगरावाली, नेपाली, बंगाली और सर....मोहम्डन भी है, खालिस मुसल्ली....कसम से सर, अरे झूठ क्यूँ बोलूँगा सर, और झूठ बोल भी दूँ तो भी क्या, सोलह साल की कुड़ी तो जवान होनी ही है....’’
‘‘क्या कहा.....? मोहम्डन भी है, तब तो हम जरूर जाएँगे....उसे पवित्र करने। यही तो जीत होगी हमारे ब्राह्मणत्व की।’’
और वे दोनों तेजी से उस अँधेरी सँकरी गली में घुस गए।
कुछ कदम और आगे ....
एक दूसरा दृश्य.....इसी से मिलता-जुलता।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book